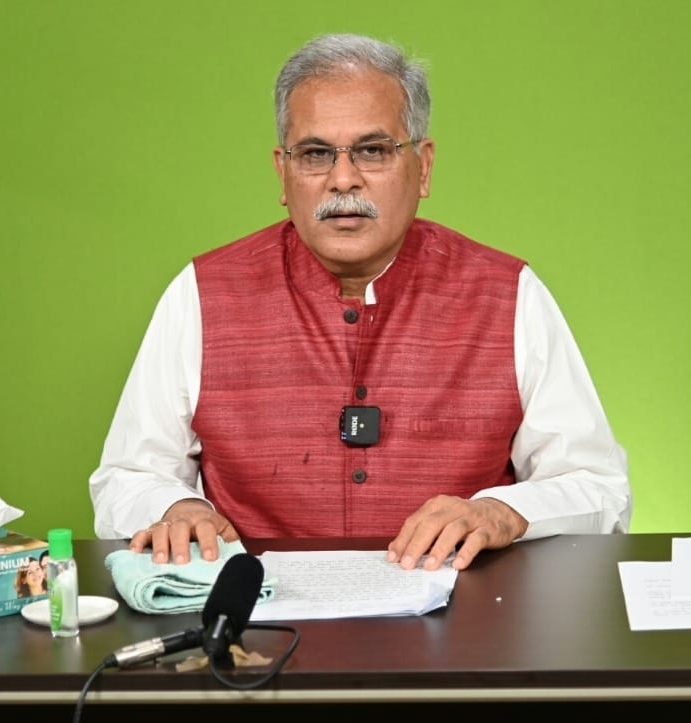इंडिया रिपोर्टर लाइव
नई दिल्ली। पड़ोसी देशों से आपसी रिश्तों के लिहाज से हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज की परिस्थितियों में यदि भारत परंपरागत नीतियों का पालन करता है, तो अपने हितों को नुकसान होता है और अगर देशहित की रक्षा करना चाहे, तो लोकतांत्रिक आस्थाएं दरकती हैं। ऐसे में यह भी सच है कि बहुमत की राय देश की दिलचस्पी के पक्ष में होगी। लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्श तो हर कालखंड में खंडित-मंडित होते रहते हैं। भारत और म्यांमार के संबंध कुछ इसी ऊहापोह का सामना कर रहे हैं। आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ कर फौज ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली है।
अब हिंदुस्तान के सामने धर्मसंकट है। वह सू की के लोकतंत्र का समर्थन करे भी, तो कैसे? सू की तो शत्रु देश चीन से हाथ मिलाकर खुल्लमखुल्ला भारत को धमका चुकी थीं। म्यांमार की सेना ने कम से कम भारत के लिए तो इतिहास में भी कभी मुसीबत नहीं खड़ी की। तब भी नहीं, जब सू की नजरबंद थीं और लोकतंत्र बहाली के लिए भारत से उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा था। सेना उन दिनों वहां बेहद ताकतवर थी। देखा जाए, तो बीते दिनों वहां हुआ तख्तापलट भारतीय हितों के नजरिये से अच्छा ही है। सू की जिस राह पर चल पड़ी थीं, वह हिंदुस्तान से दोस्ती वाली तो नहीं ही थी। यह दीगर बात है कि लोकतंत्र समर्थकों को कुचलने के लिए वहां फौज जिस तरह क्रूर और हिंसक हो रही है, उसे कोई भी सभ्य समाज अच्छा नहीं कहेगा। दो महीनों में पांच सौ से अधिक प्रदर्शनकारी सेना की गोली का निशाना बन चुके हैं। और किसी भी राष्ट्र की सेना या पुलिस जब गोली चलाती है, तो अपने-पराये का फर्क भूल जाती है।
दरअसल विदेश नीति के जानकारों को म्यांमार की इस नेत्री का व्यवहार करीब दो बरस पहले बड़ा विचित्र और अटपटा लगा था, जब भारत की तरफ साफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ देश मानवाधिकार, जातीयता और धर्म के बहाने दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। म्यांमार उन्हें कहना चाहता है कि अब वह अपने देश में ऐसा कोई हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेगा। सू की ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 33 समझौतों पर दस्तखत करने के बाद वह बात कही थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि म्यांमार बदल चुका है। अब वह भारत का पिछलग्गू नहीं रहा है और भविष्य में भारत के हितों की रक्षा की गारंटी भी नहीं लेनेवाला। सू की ने तो यहां तक कहा था कि उनका देश हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा। अपनी जवानी में भारत में पढ़ाई कर चुकीं सू की वैसे हिंदुस्तान को अपना दूसरा घर मानती रही हैं। लेकिन उन्होंने चीन के साथ कई ऐसे समझौते किए, जो भारत के सामरिक हितों के खिलाफ थे और पड़ोसियों के जरिये भारत की घेराबंदी को कामयाब बनाने की गारंटी देते थे।
ऐसी स्थिति में भारत क्या करे? लोकतंत्र-विरोधी सेना की हुकूमत को सहयोग दे, जो भारत से हमेशा बेहतर रिश्ते बनाकर रखती आई है या भारत की घनघोर विरोधी व लोकतंत्र समर्थक सू की को मजबूत करने में योगदान दे, जो उम्र भर भारत के गीत गाती रहीं और जब सरकार में बैठीं, तो चीन के पाले में चली गईं। भारत के लिए इस तरह के बांझ रिश्तों को पालने-पोसने का क्या अर्थ है, जो लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ विश्वासघात की फसल उगाते हैं? माना कि रोहिंग्या समस्या से निपटने में भारत ने कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई और चीन ने म्यांमार का बांग्लादेश के साथ गुपचुप तरीके से अमेरिका में समझौता करा दिया था। इसे लेकर म्यांमार अगर भारत के प्रति शत्रु भाव रखता है, तो कोई क्या कर सकता है? फिर तो सू की को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि आज चीन भी म्यांमार की फौज से सू की के पक्ष में नहीं बोल रहा, तो उसके क्या कारण हैं? साफ है कि भारत की चुप्पी से खफा होने का नैतिक आधार सू की खो चुकी हैं।
एक बार म्यांमार की सेना के पक्ष पर भी विचार करना जरूरी है। फौज के आरोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता कि सू की म्यांमार के हितों के खिलाफ काम कर रही थीं और भ्रष्टाचार में लिप्त थीं। सेना का यह भी आरोप है कि वह संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। चूंकि वह खुद विदेशी नागरिक से ब्याह रचाने के कारण राष्ट्रपति नहीं बन सकती थीं, इसलिए उन्होंने अपने एक कठपुतली समर्थक को राष्ट्रपति बनाया और फिर खुद को संविधान से ऊपर समझने लगी थीं। जानना दिलचस्प है कि सेना ने सू की को अंधेरे में रखकर बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं को मार डाला था, पर सू की ने संयुक्त राष्ट्र में सेना के उस कदम का बचाव किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी वैश्विक छवि खो दी थी। वह भूल गई थीं कि तिरासी फीसदी वोट दोबारा सरकार बनाने के लिए तो बहुत थे, पर संविधान के तहत सेना इससे कमजोर नहीं होती।
जाहिर है कि सू की को अब लंबे समय तक राहत नहीं मिलने वाली। वह वही फसल काट रही हैं, जो उन्होंने बोई थी। ऐसे में भारत अब उनका साथ क्यों दे? दूसरे देशों में लोकतंत्र और अखंडता हमें भली लग सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के अपने हितों की कीमत पर नहीं। एशिया की तीन बड़ी ताकतें रूस, चीन और भारत फौजी कार्रवाई पर चुप्पी साधे हैं। पश्चिम और यूरोप के देश कितना विरोध करेंगे, कहा नहीं जा सकता। आखिर हमें 1988 की याद भी तो है, जब इसी सेना ने अपने हजारों नागरिकों का कत्ल किया था और सारा विश्व देखता रहा था।